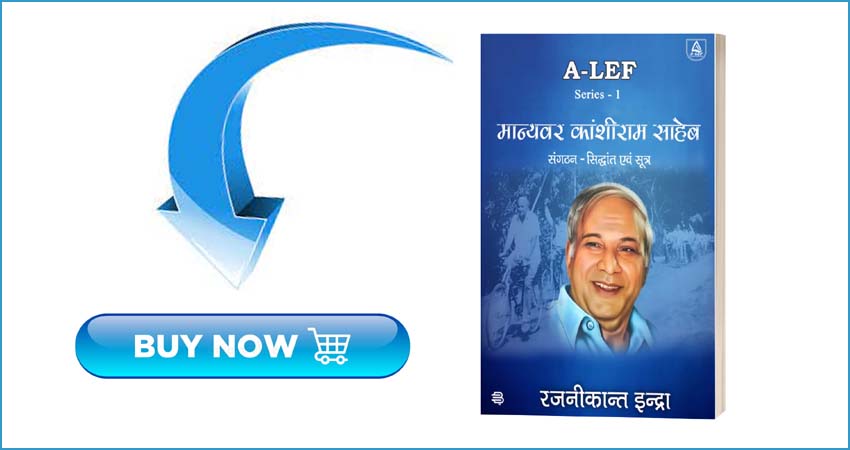भारत एक ऐसा देश है, जहाँ विविधता अपने पूर्ण वैभव में प्रस्फुरित होती है। यहाँ असंख्य भाषाएँ, धर्म और हजारों जातियाँ एक अनुपम सांस्कृतिक मोज़ेक रचती हैं। इस सामाजिक ताने-बाने में जाति एक ऐसी कड़ी है, जो वर्गीकृत व्यवस्था को आधार प्रदान करती है। लोकतंत्र, जो किसी भी राष्ट्र के शासन और प्रशासन—चाहे वह राजनीतिक हो, सामाजिक हो या आर्थिक—का प्राणतत्त्व है, समाज के प्रत्येक वर्ग के स्व-प्रतिनिधित्व और सक्रिय भागीदारी से ही सशक्त होता है। किंतु भारत के लिए यह एक विडंबना ही कही जाएगी कि यहाँ सहस्राब्दियों से सांस्कृतिक रूप से समृद्ध जातियाँ—ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य—अपने आधिपत्य के बल पर उन जातियों को हाशिये पर धकेलती आई हैं, जो सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में बहिष्करण और अत्याचार की शिकार रही हैं।
निम्न सामाजिक स्थिति वाली जातियों के समक्ष उपस्थित यह संकट अकेला नहीं है। साम्यवाद, सांप्रदायिकता, धन का दुरुपयोग, मीडिया की पक्षपातपूर्ण भूमिका, माफिया का प्रभाव और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) की संदिग्धता ने दलितों, आदिवासियों और अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) की स्वतंत्र राजनीति को पथभ्रष्ट कर दिया है। इन समस्त कुरीतियों के परिणामस्वरूप, इन वर्गों के वास्तविक प्रतिनिधियों के स्थान पर चमचे—जो स्वार्थ और अवसरवाद के दास हैं—एससी, एसटी और ओबीसी के मसीहा बनकर उभरे हैं। यह स्थिति न केवल चिंतनीय है, अपितु भारतीय लोकतंत्र की मूल भावना के लिए एक गंभीर चुनौती भी है।
स्वतंत्रता के पश्चात् पिछले सात दशकों से हमने “फर्स्ट पास्ट द पोस्ट” (प्रथम विजेता) चुनाव पद्धति को अपनाया है। इस पद्धति को स्वीकार करने का आधार उस समय की अशिक्षित जनसंख्या थी, जो स्वयं निर्णय लेने में असमर्थ मानी जाती थी। किंतु आजादी के बाद के सफर में हमने 1951 की 18.33% साक्षरता दर से 2024 में 80% साक्षरता का स्वर्णिम पड़ाव हासिल किया है। यह उपलब्धि एक मील का पत्थर है, जो हमें यह सोचने को विवश करती है कि अब हम एक नई चुनाव पद्धति की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। वर्तमान भारत में यह स्पष्ट है कि व्यक्तियों के स्थान पर राजनीतिक दल और उनकी विचारधाराएँ ही चुनावी मैदान में प्रमुखता से उतरती हैं। कुछ अपवाद अवश्य हैं, किंतु उनमें से अधिकांश अपराधी, बाहुबली और गुंडों की श्रेणी में आते हैं, जो लोकतंत्र की गरिमा को कलंकित करते हैं। ऐसी स्थिति में भारत के लिए लोकसभा, विधानसभा और पंचायतीराज स्तर पर “आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति” को अपनाना एक श्रेयस्कर विकल्प हो सकता है।
इस पद्धति के अंतर्गत मतदाता किसी व्यक्ति के बजाय एक राजनीतिक दल के लिए मतदान करते हैं, और प्रत्येक दल को प्राप्त मतों के अनुपात के आधार पर सीटें आवंटित की जाती हैं। यह व्यवस्था भारत के उन मूक वर्गों—विशेष रूप से एससी, एसटी और ओबीसी—को एक सशक्त आवाज़ प्रदान कर सकती है, जो अब तक अपने हक़ से वंचित रहे हैं। यह पद्धति न केवल समावेशिता को बढ़ावा देगी, बल्कि लोकतंत्र के उस मूल सिद्धांत को भी साकार करेगी, जिसमें प्रत्येक वर्ग की हिस्सेदारी सुनिश्चित हो। हमने पिछले सात दशकों तक “फर्स्ट पास्ट द पोस्ट” पद्धति के परिणामों को देखा और परखा है। अब “आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति” को अपनाने और इसे एक प्रयोग के रूप में लागू करने में कोई हानि नहीं है। बाबासाहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर द्वारा रचित संविधान एक जीवंत और गतिशील दस्तावेज है, जो भारत और भारतीयों के कल्याण के लिए हर संभव मार्ग प्रशस्त करता है। यह संविधान हमें परिवर्तन की स्वतंत्रता देता है, और यही इसकी महानता है।
अतः यह आवश्यक हो जाता है कि भारतीय संसद, जनता, शिक्षाविद् और सभी हितधारक इस विषय पर एक स्वस्थ और सार्थक विमर्श करें। हमें आशा है कि हम इस पद्धति को अंगीकार कर सकते हैं। यदि यह सफल होती है, तो यह भारत के लोकतंत्र के लिए एक स्वर्णिम अध्याय होगा। और यदि यह अपेक्षाओं पर खरी न उतरे, तो संविधान संसद को किसी अन्य बेहतर विकल्प की ओर बढ़ने की शक्ति प्रदान करता है। यह लचीलापन ही हमारे संवैधानिक ढांचे की प्राणशक्ति है। इस प्रकार, समय आ गया है कि हम अपनी सहस्राब्दियों पुरानी सामाजिक कुरीतियों को चुनौती दें और एक ऐसी व्यवस्था की नींव रखें, जो वास्तव में समता, स्वतंत्रता और न्याय के आदर्शों पर आधारित हो। “आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति” इस दिशा में एक साहसिक कदम हो सकता है, जो भारत के हाशिये पर पड़े वर्गों को उनके अधिकारों का सच्चा भागीदार बनाए।