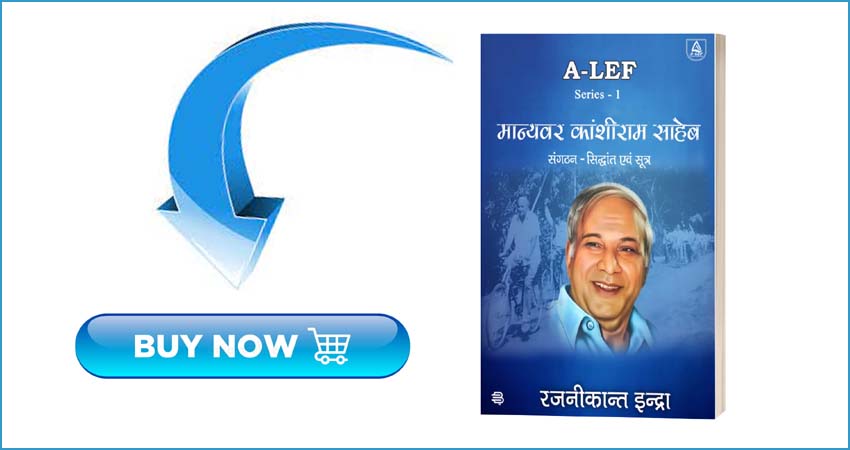भारतीय संस्कृति में दो राम: निर्गुण बनाम सगुण का दार्शनिक और सामाजिक विश्लेषण
भारतीय संस्कृति में ‘राम’ के दो अलग-अलग स्वरूपों का उल्लेख मिलता है, जो न केवल दार्शनिक आधार पर एक-दूसरे से भिन्न हैं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों में भी गहरे अंतर को उजागर करते हैं। एक ओर हैं जगतगुरु रैदास और कबीर के निर्गुण, निराकार राम, जो समय, रूप और गुणों से परे हैं। दूसरी ओर हैं कवि वाल्मीकि और तुलसीदास के सगुण श्रीराम, जो मानवीय गुणों, जन्म-मृत्यु और परिवर्तन के अधीन हैं। इन दोनों के बीच का अंतर केवल दर्शन का विषय नहीं, बल्कि यह जातिवादी और मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ संत परंपरा के संघर्ष का भी प्रतीक है।
निर्गुण राम : रैदास और कबीर का दर्शन
जगतगुरु संत शिरोमणि रैदास और कबीरदास के राम एक ऐसी सत्ता हैं, जो न शक्ल रखते हैं, न सूरत। इनका न रंग है, न रूप। ये जन्म और मृत्यु से मुक्त, सुख-दुख से परे, कण-कण में व्याप्त हैं। ये न सृष्टि के सृजनकर्ता हैं, न संचालक, न संहारक। ये निर्गुण, निराकार और समय से आजाद हैं—एक अपरिवर्तनीय सत्य। रैदास इस अंतर को स्पष्ट करते हुए कहते हैं:
रैदास हमारे रामजी, दशरथ का सूत नाहीं।
राम रम रह्यों हमीं में, बसै कुटुम्ब माहीं।।
अर्थात, उनके राम दशरथ के पुत्र श्रीराम नहीं, बल्कि वह चेतना हैं जो हर प्राणी के भीतर निवास करती है, जिसमें सारा संसार एक परिवार की तरह समाहित है। इसी तरह कबीर कहते हैं:
कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढ़े वन माहि।
ऐसे घट-घट राम हैं दुनिया खोजत नाहिं।।
यहां कबीर के राम वह सत्य हैं जो भीतर बसता है, जिसे लोग बाहर खोजते फिरते हैं। कबीर सगुण ईश्वर की सभी संकल्पनाओं—ईश्वर, नारायण, हरि, राम, कृष्ण, ब्रह्मा, विष्णु, महेश—को कल्पना मात्र बताकर खारिज करते हैं:
ईश्वर, नारायण, हरि, राम, कृष्ण, घनश्याम।
ब्रम्हा, विष्णु, महेश, सब कल्पित नाम।।
रैदास भी श्रीराम को नकारते हुए कहते हैं:
राम न जानूँ, न भगत कहाऊँ, सेवा करूँ न दासा।
योग, यज्ञ, गन न जानूँ, तातें रहूँ उजासा।।
यहां वे दशरथ के पुत्र श्रीराम, उनकी भक्ति और ब्राह्मण धर्म के कर्मकांडों को अस्वीकार करते हैं, और ज्ञान के प्रकाश को अपनाते हैं। रैदास यह भी कहते हैं:
जाति ओछी पाँति ओछी, ओछा जन्म हमारा।
राजा राम की सेवा न किन्हीं, कहैं रैदास चमारा।।
यहां वे जातिवादी व्यवस्था के श्रीराम को स्पष्ट रूप से खारिज करते हैं, जो उन्हें उनके जन्म के आधार पर निम्न मानती है। इस तरह रैदास और कबीर का राम एक सर्वव्यापी, समतामूलक और जाति-धर्म से मुक्त सत्य का प्रतीक है।
सगुण श्रीराम : वाल्मीकि और तुलसी की रचना
दूसरी ओर, वाल्मीकि और तुलसीदास के श्रीराम एक मानवीय स्वरूप हैं। वाल्मीकि की संस्कृत रामायण और तुलसीदास के अवधी रामचरितमानस में श्रीराम दशरथ के पुत्र हैं—सांवले, सुंदर, जन्म और मृत्यु के चक्र में बंधे। वे सुख-दुख का अनुभव करते हैं: माता-पिता और पत्नी से बिछड़ने पर दुखी होते हैं, मिलने पर प्रसन्न। वे प्रजजन के हिस्से हैं (लव-कुश उनके पुत्र), पालन-पोषण में भागीदार हैं, और अपने हितों के लिए शंबूक, बाली और रावण जैसे पात्रों का संहार करते हैं। ये सगुण हैं, आकार और समय के अधीन हैं। वे शिशु से युवा, फिर वृद्ध होते हैं और अंततः मृत्यु को प्राप्त होते हैं। अर्थात, वे अस्थिर हैं, स्थायी सत्य नहीं।
वाल्मीकि की रामायण, जो जातक कथाओं से प्रेरित है, और तुलसी की भक्ति-प्रधान रचना ने श्रीराम को ईश्वर का दर्जा दिया। यह लेखन की शक्ति का उदाहरण है, जिसने एक काल्पनिक चरित्र को सामाजिक चेतना में स्थापित कर दिया।
जातिवादी षड्यंत्र और संत परंपरा का संघर्ष
इन दो रामों के बीच का अंतर केवल दार्शनिक नहीं, बल्कि सामाजिक संघर्ष का भी परिचायक है। जातिवादियों और मनुवादियों ने बुद्ध, रैदास और कबीर की निर्गुण परंपरा को मिटाने के लिए सुनियोजित प्रयास किए। इस षड्यंत्र के तहत रैदास और कबीर को भक्ति आंदोलन से जोड़कर उनके ज्ञानमार्गी दर्शन को तोड़-मरोड़ दिया गया। चमत्कारिक कहानियां गढ़ी गईं, और उनके निर्गुण राम को वाल्मीकि-तुलसी के सगुण श्रीराम के साथ एक करने की कोशिश की गई। यह प्रयास कुछ हद तक सफल भी हुआ, क्योंकि आम जनमानस में यह भ्रम फैल गया कि दोनों राम एक ही हैं।
लेकिन रैदास और कबीर ने इस षड्यंत्र को अपने दर्शन के प्रकाश से नष्ट कर दिया। रैदास ने स्पष्ट किया कि उनके राम दशरथ के पुत्र नहीं, बल्कि वह सत्य हैं जो कण-कण में व्याप्त है। कबीर ने सगुण ईश्वर की अवधारणा को कल्पना कहकर खारिज किया। यह संत परंपरा का वह उजाला था, जिसने जातिवादी अंधेरे को चीर दिया।
दो रामों का अंतर और सामाजिक संदर्भ
एससी, एसटी और ओबीसी जैसे वंचित समुदायों के लोक जीवन में राम निर्गुण हैं—वह सत्य जो समता और स्वतंत्रता का प्रतीक है। वहीं, वाल्मीकि-तुलसी के श्रीराम सगुण हैं, जो एक विशेष सामाजिक व्यवस्था और शक्ति संरचना का प्रतिनिधित्व करते हैं। ‘राम-राम’ का उच्चारण निर्गुण सत्य की ओर संकेत करता है, जबकि ‘जय श्रीराम’ या ‘जय सिया वर राम’ सगुण श्रीराम की भक्ति को रेखांकित करता है। इन दोनों के दर्शन में जमीन-आसमान का अंतर है।
इन दोनों को एक मानना न केवल इतिहास के साथ अन्याय है, बल्कि संत परंपरा के संघर्ष को भी नजरअंदाज करना है। निर्गुण राम जाति और धर्म की सीमाओं से मुक्त हैं, जबकि सगुण श्रीराम एक ऐसी व्यवस्था का हिस्सा हैं, जिसे मनुवादियों ने अपने हितों के लिए रचा।
निष्कर्ष :
भारतीय संस्कृति में दो रामों की अवधारणा दर्शन और समाज के दो ध्रुवों को दर्शाती है। रैदास और कबीर का निर्गुण राम समता, स्वतंत्रता और सत्य का प्रतीक है, जो जातिवादी बंधनों को तोड़ता है। वहीं, वाल्मीकि और तुलसी का सगुण श्रीराम एक साहित्यिक और धार्मिक रचना है, जो समय और परिवर्तन के अधीन है। इन दोनों को एक समझना संतों के दर्शन और उनके संघर्ष को कमजोर करता है। यह समझना जरूरी है कि निर्गुण राम वह प्रकाश हैं, जो मनुष्य को भीतर के सत्य तक ले जाते हैं, जबकि सगुण श्रीराम एक ऐसी कथा का हिस्सा हैं, जिसे शक्ति और वर्चस्व के लिए गढ़ा गया। इन दोनों के बीच का अंतर ही संत परंपरा की क्रांतिकारी विरासत को जीवित रखता है।