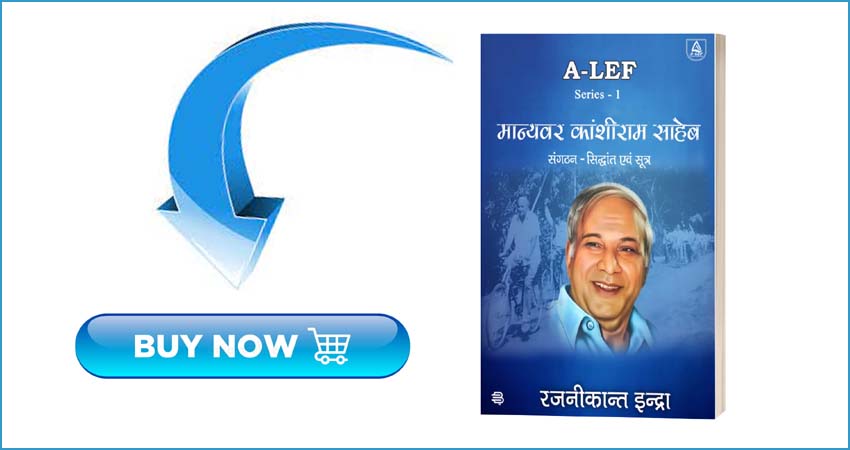भारतीय समाज की सबसे गहरी और लगभग अटूट बीमारी उसकी जाति-आधारित ऊँच-नीच की मानसिकता है, जिसे विद्वान व विचारक “ब्रह्मणी रोग” या ब्राह्मणवादी चेतना का मूल स्वरूप कहते हैं। इस व्यवस्था में हर व्यक्ति, चाहे वह सामाजिक सीढ़ी पर कितना भी नीचे क्यों न हो, अपने से भी नीचे किसी को ढूँढकर अपनी पहचान को सांत्वना देता है। दलितों की सभी जातियां अपने से भी अधिक दलित या अन्य अस्पृश्य (चमार/महार आदि) समुदाय को देखकर संतुष्ट होता है, पिछड़ा अपने से नीचे ओबीसी या दलित को देखकर खुद को ऊँचा समझता है, और सवर्ण अपने से नीचे सभी को देखकर अपनी श्रेष्ठता की पुष्टि करता है। यह एक अनंत श्रृंखला है जिसमें संतुष्टि का आधार हमेशा “दूसरे की निम्न सामाजिक स्थिति” होता है, न कि अपनी वास्तविक उपलब्धि, नैतिकता या मानवीय गरिमा।
यह व्यवस्था केवल सामाजिक पदानुक्रम की बात नहीं करती, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक संकट पैदा करती है। व्यक्ति अपनी असुरक्षा, हीनभावना और आत्म-सम्मान की कमी को दूसरों को नीचा दिखाकर पूरा करने की कोशिश करता है। समाजशास्त्रियों ने इसे “सापेक्ष अभाव की भावना” (relative deprivation) से जोड़ा है, परंतु भारतीय संदर्भ में यह भावना जन्मजात और धार्मिक रूप से वैध बनाई गई है। मनुस्मृति, गीता, पुरूष सूत्र से लेकर लोक परंपराओं तक, ऊँच-नीच का यह ढाँचा इतना गहरा बैठ गया है कि आज भी शिक्षा, शहरीकरण और आर्थिक प्रगति के बावजूद भारतीयों की अंतःचेतना में यह सक्रिय रहती है।
इस रोग का मूल स्रोत ब्राह्मणवाद है, क्योंकि इसने न केवल सामाजिक विभाजन को जन्म दिया, बल्कि उसे दैवीय और नैसर्गिक सिद्ध करने का दार्शनिक ढाँचा भी तैयार किया। वर्ण व्यवस्था को जन्म-आधारित पदक्रम में बदलने के बाद यह विचार स्थापित हो गया कि ऊँचाई-नीचाई कर्म से नहीं, बल्कि जन्म से तय होती है। इसीलिए आज भी जब कोई व्यक्ति कहता है “हम तो ऊँची जाति के हैं”, तो वह वास्तव में अपनी व्यक्तिगत योग्यता का नहीं, बल्कि अपने पूर्वजों द्वारा किसी अन्य समूह पर थोपी गई व्यवस्था का प्रमाण-पत्र पेश कर रहा होता है।
यह “अपने से नीचे किसी को ढूँढने” की प्रवृत्ति भारतीय समाज को एकजुट होने से रोकती है। जब तक व्यक्ति अपनी गरिमा को दूसरों की हीनता में तलाशता रहेगा, तब तक वास्तविक समानता, सामूहिक प्रगति और मानवीय संवेदना का विकास लगभग असंभव रहेगा। यह ब्रह्मणी रोग केवल सामाजिक बुराई नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक आत्म-घात है जो सदियों से भारतीय समाज की रीढ़ को खोखला करता आ रहा है।
सच्ची मुक्ति तभी संभव है जब हम “ऊँच-नीच” की इस बीमार मानसिकता को त्यागकर यह स्वीकार करें कि हर मनुष्य का मूल्य उसके जन्म से नहीं, बल्कि उसके कर्म, करुणा और चेतना से तय होता है। जब तक यह परिवर्तन नहीं होगा, तब तक भारत में असली लड़ाई वर्ग, धर्म या राजनीति की नहीं — बल्कि “ऊँच बनाम नीच” की ही रहेगी। और दुर्भाग्य से, इस लड़ाई में हर कोई हार रहा है, मानवता हार रही है— क्योंकि इस व्यवस्था में कोई भी वास्तव में जीत नहीं सकता।