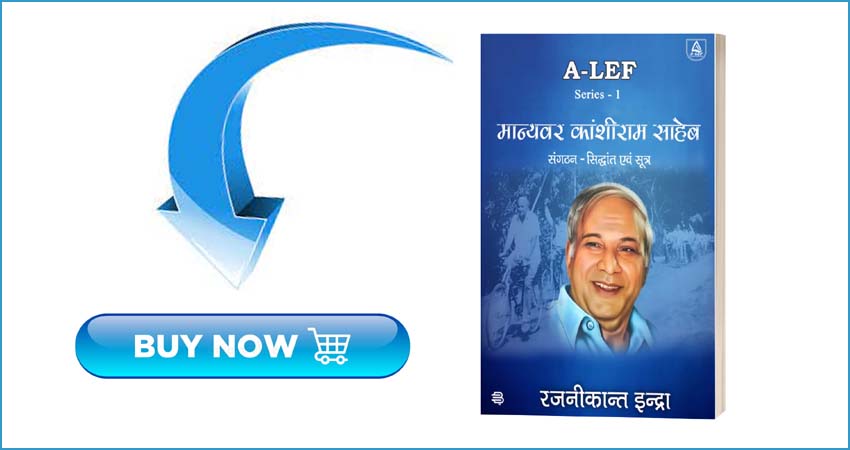समता और समरसता दो ऐसे शब्द हैं जो भारतीय सामाजिक और दार्शनिक संदर्भ में गहरे अर्थ रखते हैं। ये दोनों अवधारणाएं सामाजिक व्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखती हैं, लेकिन इनके उद्देश्य, दृष्टिकोण और प्रभाव में मौलिक अंतर है। इस लेख में इनके बीच अंतर को स्पष्ट करते हुए यह विश्लेषण किया जाएगा कि भारत को वर्तमान में किसकी अधिक आवश्यकता है।
1. समता और समरसता की परिभाषा
समता: समता का तात्पर्य ‘समानता—सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर सभी व्यक्तियों के लिए एक समान अवसर और अधिकार’ है। यह संरचनात्मक असमानताओं को दूर करने और हर व्यक्ति को समान मंच प्रदान करने की अवधारणा है। समता संविधान के मूल सिद्धांतों में से एक है, जो अनुच्छेद 14 (कानून के समक्ष समानता) और अनुच्छेद 15 (भेदभाव का निषेध) में प्रतिबिंबित होती है। भारतीय सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में समता सामाजिक परिवर्तन के द्वारा जाति उन्मूलन कर समतामूलक समाज सृजन करना चाहती है।
समरसता : समरसता का अर्थ ‘भारत के संदर्भ में जाति व्यवस्था को यथावत कायम रखते हुए सामाजिक सद्भाव, एकता और आपसी सहयोग’ है। यह समाज के विभिन्न वर्गों, जातियों, धर्मों और समुदायों के बीच वैमनस्य को कम करके एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने पर केंद्रित है। समरसता भावनात्मक और सामाजिक एकजुटता पर जोर देती है, जिसमें मतभेदों एवं जातिगत भेदभाव को स्वीकार करते हुए साथ रहने की भावना विकसित की जाती है। भारतीय सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में समरसता जाति व्यवस्था को कायम रखना चाहती है।
2. समरसता और समता में अंतर
| क्रम संख्या | तुलना का आधार | समरसता (भारत के संदर्भ में) | समता (भारत के संदर्भ में) |
| 1 | लक्ष्य | सामाजिक एकता, सौहार्द संग जाति व्यवस्था को यथावत बनाये रखना | सामाजिक परिवर्तन द्वारा जाति उन्मूलन कर संरचनात्मक समानता, न्याय को स्थापित करते हुए समतामूलक समाज सृजन करना |
| 2 | बंधुत्व | कोई गारंटी नहीं | गारंटी |
| 3 | स्वतंत्रता | कोई गारंटी नहीं | गारंटी |
| 4 | दृष्टिकोण | भावनात्मक, सह-अस्तित्व पर आधारित | अधिकार और अवसरों की समानता पर आधारित |
| 5 | प्रकृति | मौजूदा विविधता को स्वीकार करना | असमानताओं को समाप्त करना |
| 6 | उदाहरण | विभिन्न जातियों का एक साथ उत्सव मनाना | सभी को समान शिक्षा और नौकरी के अवसर |
| 7 | आवश्यकता | सहानुभूति और आपसी समझ | नीतिगत और कानूनी सुधार |
संक्षेप में, समरसता समाज “जैसा है, वैसा ही रहे” को स्वीकार करते हुए उसे जोड़ने की कोशिश करती है, जबकि समता समाज को “जैसा होना चाहिए” की ओर ले जाती है। समरसता मतलब ‘यथास्थिति (जाति व्यवस्था) को क़ायम रखना‘ जबकि समता का मतलब ‘सामाजिक परिवर्तन द्वारा जाति उन्मूलन कर समतामूलक समाज सृजन करना’ है।
3. भारत को किसकी ज्यादा जरूरत है?
भारत एक बहु-सांस्कृतिक, बहु-जातीय और बहु-धार्मिक राष्ट्र है, जहां सामाजिक असमानताएं और विविधताएं दोनों ही गहरे रूप से मौजूद हैं। इस संदर्भ में, समरसता और समता दोनों की अपनी-अपनी प्रासंगिकता है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में भारत को ‘समता’ की अधिक आवश्यकता है। इसके पीछे निम्नलिखित कारण हैं:
- ऐतिहासिक असमानताएं : भारत में जाति व्यवस्था, लैंगिक भेदभाव और आर्थिक विषमता ने समाज के बड़े हिस्से को अवसरों से वंचित रखा है। उदाहरण के लिए, दलितों और आदिवासियों की साक्षरता और रोजगार दर अभी भी राष्ट्रीय औसत से कम है। समता इन संरचनात्मक असमानताओं को दूर करने का एकमात्र रास्ता है।
- सामाजिक न्याय का आधार : संविधान निर्माता डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने समता को भारत के लोकतंत्र की नींव माना। आरक्षण, शिक्षा और रोजगार में समान अवसर जैसे कदम समता के बिना संभव नहीं हैं। बिना समानता के, सामाजिक न्याय एक खोखला नारा बनकर रह जाता है।
- आर्थिक विकास : भारत को वैश्विक शक्ति बनने के लिए अपने सभी नागरिकों की क्षमता का उपयोग करना होगा। समता के अभाव में, गरीबी और शिक्षा की कमी जैसे मुद्दे आर्थिक प्रगति को बाधित करते हैं। समान अवसर ही मानव संसाधन को सशक्त बना सकते हैं।
- कानूनी और नीतिगत जरूरत : समरसता भावनात्मक एकता ला सकती है, लेकिन यह जातिगत हिंसा, भेदभाव और आर्थिक असमानता जैसे गहरे मुद्दों को हल नहीं कर सकती। इसके लिए समता-आधारित नीतियां जैसे आरक्षण, मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं जरूरी हैं।
समरसता की सीमाएं
समरसता एक आदर्श स्थिति है, लेकिन यह अकेले पर्याप्त नहीं है। यदि समाज में संरचनात्मक असमानताएं बनी रहेंगी—जैसे कि एक समुदाय को शिक्षा और नौकरी से वंचित रखा जाए—तो केवल सामाजिक एकता, सौहार्द की बात करना सतही होगा। समरसता तभी सार्थक है जब यह समता की नींव पर खड़ी हो। उदाहरण के लिए, यदि दो समुदायों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर गहरा है, तो उनकी एकता केवल दिखावटी होगी, वास्तविक नहीं।
संतुलित दृष्टिकोण
हालांकि समता प्राथमिक आवश्यकता है, समरसता को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत की विविधता को बनाए रखने के लिए समुदायों के बीच आपसी सम्मान और सहयोग जरूरी है। समता इन असमानताओं को कम करके समरसता के लिए आधार तैयार करती है। समता समरसता की गारंटी है लेकिन इसका उल्टा सही नहीं है। इसलिए समता पहला और अनिवार्य कदम है।
4. निष्कर्ष
समरसता और समता में अंतर उनके लक्ष्य और दृष्टिकोण में निहित है — जहां समरसता समाज को जोड़ती है, वहीं समता उसे समान बनाती है। भारत को वर्तमान में समता की अधिक जरूरत है, क्योंकि बिना संरचनात्मक समानता (सामाजिक परिवर्तन एवं आर्थिक मुक्ति) के सामाजिक एकता एवं सद्भाव अधूरा और अस्थायी होगा। समता से ही समतामूलक समाज सृजन संभव है, समरसता से नहीं। समता के माध्यम से शिक्षा, रोजगार और अधिकारों में समानता लाकर ही भारत एक मजबूत, एकजुट और न्यायपूर्ण राष्ट्र बन सकता है। इसके बाद ही समरसता अपने पूर्ण रूप में फल-फूल सकेगी। इसीलिए, समता भारत के राष्ट्रनिर्माण और प्रगति का प्राथमिक एवं अनिवार्य आधार है।