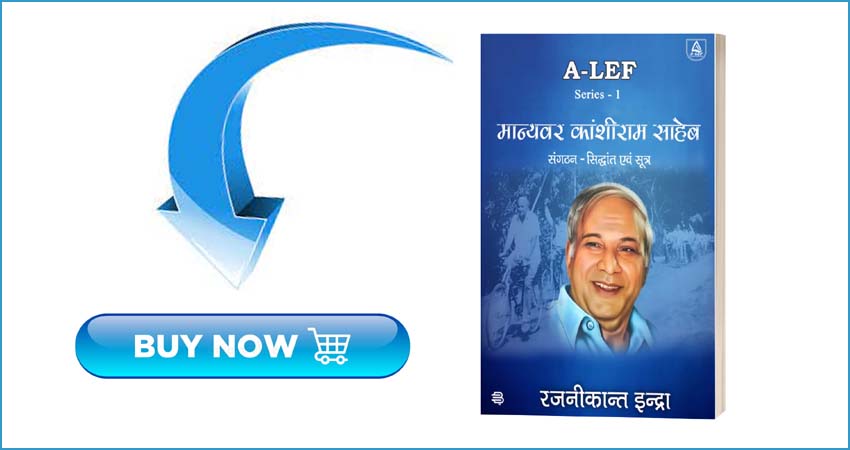राम और श्रीराम : निर्गुण बनाम सगुण का दार्शनिक और सामाजिक विश्लेषण
भारतीय संस्कृति और परंपरा में ‘राम’ शब्द दो अलग-अलग संदर्भों में प्रकट होता है—एक निर्गुण राम के रूप में, जो रैदास और कबीर के दर्शन से जुड़ा है, और दूसरा सगुण श्रीराम के रूप में, जो वाल्मीकि और तुलसीदास की साहित्यिक रचनाओं का हिस्सा है। इन दोनों के बीच का अंतर केवल शब्दों का खेल नहीं, बल्कि यह दो विचारधाराओं, जीवन-शैलियों और सामाजिक व्यवस्थाओं का प्रतिबिंब है। जहां रैदास-कबीर का राम बौद्ध दर्शन से प्रेरित समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का प्रतीक है, वहीं वाल्मीकि-तुलसी का श्रीराम सगुण भक्ति और विषमतावादी व्यवस्था का आधार है।
रैदास-कबीर के निर्गुण राम : बौद्ध परंपरा का प्रतिबिंब
रैदास और कबीर के राम एक ऐसी सत्ता हैं जो कण-कण में व्याप्त है—निर्गुण, निराकार और समय से परे। ये न सृष्टि के सृजनकर्ता हैं, न संचालक, न संहारक। इनका कोई रंग-रूप, जन्म-मृत्यु नहीं है। ये राम एक पदवी हैं, जैसे बुद्ध या बोधिसत्व—एक आध्यात्मिक अवस्था, जिसका कोई परिवार नहीं होता। यह पदवी वह व्यक्ति धारण कर सकता है जो इसके योग्य हो, लेकिन पदवी स्वयं पारिवारिक बंधनों से मुक्त होती है।
रैदास और कबीर का यह राम भारत की बौद्ध जीवन-शैली से गहराई से जुड़ा है। बुद्ध के समान, इनके राम के गुणों में सृजन, संचालन या संहार शामिल नहीं है। ये ना तो सर्वज्ञ हैं, ना सर्वत्र और ना ही सर्वशक्तिमान हैं। निर्गुण विश्लेषण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि रैदास-कबीर के राम बुद्ध का ही एक रूप हैं—एक ऐसा सत्य जो इहलोक में निहित है और परलोक की कल्पना को खारिज करता है। इस परंपरा में अनुयायियों को स्वतंत्र चिंतन और विचार की पूरी आजादी है। यहां आलोचना न केवल स्वीकार्य, बल्कि एक विशेष अंग है। यहाँ कोई ऐसा काव्य या साहित्य नहीं है जिसका आलोचनात्मक अध्ययन वर्जित हो। यह परंपरा इहलोक की वास्तविकता को महत्व देती है और परलोक में विश्वास नहीं रखती। आम जन के अभिवादन में प्रयोग होने वाला ‘राम-राम’ इसी निर्गुण राम का प्रतीक है, जो लोक जीवन में गहराई से समाया हुआ है।
वाल्मीकि-तुलसी के सगुण श्रीराम : साहित्य और भक्ति का निर्माण
दूसरी ओर, वाल्मीकि और तुलसीदास के श्रीराम सगुण हैं। ‘श्री’ शब्द गुणवाचक और सम्मानसूचक है, जो किसी रंग-रूप और कार्य से युक्त व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है। वाल्मीकि की रामायण, जो जातक कथाओं से प्रेरित है, और तुलसीदास की रामचरितमानस में श्रीराम दशरथ के पुत्र, सांवले रंग के, जन्म-मृत्यु के चक्र में बंधे एक मानवीय चरित्र हैं। वाल्मीकि के श्रीराम एक काव्य के किरदार हैं, जो अपने स्वार्थ के लिए शंबूक जैसे विद्वान ऋषि की हत्या करते हैं। यह वाल्मीकि की रचनात्मकता और कल्पनाशीलता का परिणाम है कि जातक कथाओं से प्रेरित इस काव्य ने एक बेहतरीन साहित्यिक रूप लिया, जो भारत से लेकर दक्षिण-पूर्व एशिया तक फैल गया।
तुलसीदास ने इसे एक कदम आगे ले जाकर श्रीराम को ईश्वर का दर्जा दिया। जनश्रुतियों के अनुसार, मुगल काल में तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की, लेकिन यह वाल्मीकि की रामायण का महज अनुवाद नहीं था। यह एक सुनियोजित प्रयास था, जिसमें एक सामान्य नायक को ईश्वर के रूप में स्थापित किया गया। कुछ विद्वानों का मानना है कि ‘तुलसीदास’ एक छद्म नाम हो सकता है और यह रचना कई कवियों के सामूहिक प्रयास का परिणाम है, क्योंकि एक नायक को ईश्वर बनाना किसी एक कवि की क्षमता से परे है। वाल्मीकि के श्रीराम एक आम इंसान की तरह हंसते-रोते हैं, सुख-दुख का अनुभव करते हैं, जबकि तुलसी के श्रीराम विष्णु के अवतार हैं, जिनके गुणों में सृजन, संचालन और संहार शामिल हैं। ये सर्वज्ञ, सर्वत्र एवं सर्व शक्तिमान हैं।
फिर भी, दोनों के श्रीराम सगुण हैं। ये महलों में रहते हैं, आज मंदिरों में मिलते हैं, नौकर-चाकर और दास रखते हैं, सपत्नीक हैं। इनके भक्तों को स्वतंत्र चिंतन की अनुमति नहीं है। रामायण और रामचरितमानस का आलोचनात्मक अध्ययन करना पाप माना जाता है। ये परंपरा इहलोक को मिथ्या और परलोक को सत्य मानती है। अभिवादन में ‘जय श्रीराम’ ‘जय राम’ या ‘सीता-राम’ का प्रयोग इसी सगुण श्रीराम से जुड़ा है।
दो रामों का मूल और सामाजिक संदर्भ
रैदास-कबीर के निर्गुण राम का संबंध बौद्ध परंपरा और समतामूलक जीवन-शैली से है। यह राम वह सत्य है जो कण-कण में बस्ता है और आम जन के ‘राम-राम’ में जीवित है। यह परंपरा बुद्ध, रैदास और कबीर के अनुयायियों में आज भी गांव-देहात में देखी जा सकती है। दूसरी ओर, वाल्मीकि-तुलसी का सगुण श्रीराम साहित्यिक रचना और भक्ति आंदोलन का परिणाम है, जो एक विषमतावादी (जाति) व्यवस्था को मजबूत करता है। ‘जय श्रीराम’ का प्रयोग इस व्यवस्था के पैरोकारों द्वारा किया जाता है, जो श्रीराम को शक्ति और वर्चस्व का प्रतीक मानते हैं।
रामायण का मूल जातक कथाओं में निहित है, जो बौद्ध साहित्य का हिस्सा हैं। यह उल्लेखनीय है कि वाल्मीकि, श्रीराम और रामायण गौतम बुद्ध के काल से बहुत बाद के हैं। वाल्मीकि ने अपनी विद्वता से एक काल्पनिक काव्य रचा, जिसे तुलसी ने भक्ति के रंग में रंगकर ईश्वरीय बना दिया। लेकिन निर्गुण राम की अवधारणा बौद्ध दर्शन से पहले से मौजूद थी, जिसे रैदास और कबीर ने आगे बढ़ाई।
निष्कर्ष
राम और श्रीराम दो अलग-अलग दार्शनिक और सामाजिक ध्रुवों का प्रतिनिधित्व करते हैं। रैदास-कबीर का निर्गुण राम बौद्ध परंपरा से प्रेरित समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और इहलोक का प्रतीक है, जो ‘राम-राम’ के अभिवादन में जीवित है। वहीं, वाल्मीकि-तुलसी का सगुण श्रीराम साहित्यिक रचना और भक्ति का उत्पाद है, जो ‘जय श्रीराम’ के नारे में व्यक्त होता है और विषमतावादी व्यवस्था को पोषित करता है। निर्गुण राम चिंतन और आलोचना की आजादी देता है, जबकि सगुण श्रीराम भक्ति और अधीनता की मांग करता है। इन दोनों को एक मानना न केवल दार्शनिक भूल होगी, बल्कि यह रैदास-कबीर की क्रांतिकारी परंपरा के साथ अन्याय भी होगा। आज भी गांवों में ‘राम-राम’ कहने वाले निर्गुण राम की विरासत को जीते हैं, जो बुद्ध के समान एक शाश्वत सत्य का प्रतीक है या यूं कहें कि बुद्ध के तमाम नामों में से एक नाम है।